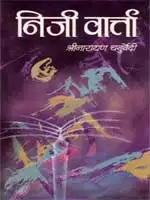|
संस्मरण >> निजी वार्त्ता निजी वार्त्ताश्रीनारायण चतुर्वेदी
|
342 पाठक हैं |
|||||||
हिंदी के राष्ट्रभाषा पद तक पहुँचने की व्यथा-कथा ही इस पुस्तक का प्रमुख कथ्य है।
प्रस्तुत हैं पुस्तक के कुछ अंश
मैंने इन संस्मरणों को अपने उत्तराधिकारयों के लिए लिखा है। मेरे
उत्तराधिकारी कौन हैं ? मेरे वंशज मेरे कानूनी उत्तराधिकारी मात्र हैं। वे
मेरी भौतिक संपत्ति के (जो नगण्य है) उत्तराधिकारी हैं; किन्तु मेरे
वास्तविक उत्तराधिकारी वे भावी युवक हैं जिनमें हिंदी-प्रेम ही नहीं,
हिंदी का दर्द भी हो; वे नहीं जो मात्र साहित्य-रचना कर या संपादन या
हिंदी अध्यापन कर अपना पेट पालते हों और इसी को हिन्दी-सेवा समझते हों।
मेरे उत्तराधिकारी वे होंगे जो हिंदी के हितों, हिंदीभाषियों और हिंदी की
सेवा करने वालों के हितों के लिए निस्पृह भाव से कार्य करें और हिंदी-भक्त
साहित्यकारों की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास करें और हिंदी के लिए
त्याग और कठिन परीक्षा देने को तैयार हों और जो हिंदी के मान की प्राणपण
से रक्षा करें तथा हिंदी का
‘अलमबरदार’ होना गौरव की बात समझें।
‘अलमबरदार’ तो आज अनेक हैं पर वास्तव में हिंदी के प्रति उनकी आस्था कितनी हैं, यह संदिग्ध है। ‘जो घर फूँके आपना’ का भाव हिंदी हित के लिए जिसका होगा,वही भैया साहब का सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। क्योंकि भैया साहब ही थे जिनके त्याग और तपस्या से आज भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के राष्ट्रभाषा पद तक पहुँचने की व्यथा-कथा ही इस पुस्तक का प्रमुख कथ्य है।
‘अलमबरदार’ होना गौरव की बात समझें।
‘अलमबरदार’ तो आज अनेक हैं पर वास्तव में हिंदी के प्रति उनकी आस्था कितनी हैं, यह संदिग्ध है। ‘जो घर फूँके आपना’ का भाव हिंदी हित के लिए जिसका होगा,वही भैया साहब का सच्चा उत्तराधिकारी हो सकता है। क्योंकि भैया साहब ही थे जिनके त्याग और तपस्या से आज भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी के राष्ट्रभाषा पद तक पहुँचने की व्यथा-कथा ही इस पुस्तक का प्रमुख कथ्य है।
लेखकीय निवेदन
ये अन्तरंग संस्मरण मैंने बहुत दिनों हेमलेट की तरह ‘करूँ या न
करूँ’ की दुविधा में फँसे रहने के बाद लिखे हैं। इन्हें लिखने में
मुझे बहुत आगा-पीछा सोचना पड़ा। संविधान में हिन्दी को राजभाषा पद पर
प्रतिष्ठित करने में अपने महत्त्वपूर्ण सहयोग या प्रौढ़ों को रोमन लिपि
द्वारा हिंदी सिखाने से मेरा इनकार, जिसने एक वैयक्तिक झगड़े का रूप ले
लिया, यदि किसी से कहता तो ‘अपने मुँह तुम आपन करनी’ की तरह
अशोभनीय मालूम होता। दूसरे अधिकांश लोग समझते कि मैं जीट हाँक रहा हूँ और
वे शायद मेरा विशवास न करते; अगर करते भी तो अंग्रेजी की कहावत के अनुसार-
‘‘With a spoonful or bucketful of salt’
इसका कारण यह था कि मेरे पास इन प्रकरणों के लिए कोई प्रमाण न था। यदि मित्रवत पं. बलभद्र मिश्र ने उस प्रकरण के संबंध में लेख न लिखा होता जो उन्होंने लिखकर मुझे कहीं छापने के लिए दिया था (मैंने सेवा) में होने के कारण उसे उस समय छापना उचित नहीं समझा था) तथा 1976 में मित्रों द्वारा स्नेहवश प्रयाग में आयोजित सारस्वत समारोह के अवसर पर भाई सीताराम जाजू के हिन्दुस्तानी अकादमी के सचिव पं. उमाशंकर शुल्क को वह पत्र न भेजा होता जो मैंने अपने लेख में उद्धृत किया है (और जिसकी एक प्रतिलिपि हाथ से लिखकर मुझे भेजी), तो उसे मैं नहीं लिखता। मौखिक रूप से मैंने इनकी चर्चा (विशेषकर श्री जाजूवाले प्रसंग की) किसी से नहीं की किन्तु अब उन घटनाओं की सप्रमाण (विश्वासनीय व्यक्तियों की लिखित) साक्षी मिल जाने पर ही मैंने उन्हें लिपिबद्ध किया है। ऐसे अन्य प्रसंग भी हैं; किंतु मेरे पास उनके संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं। यदि वे लोगों को कुछ मनोरंजन करें या कुछ प्रेरणा दें तो मेरे लिए पर्याप्त है।
हिन्दी की सेवा का अर्थ केवल साहित्य रचना नहीं है। मैंने अपने विचार से जिस काम को हिंदी के हित में समझा, वह किया।
साहित्य-रचना के क्षेत्र में मेरा काम उल्लेखनीय है या नहीं अथवा मेरा संपादन किसी काम का है या नहीं, इसकी चिंता मुझे नहीं। जिस हिंदी संसार ने श्रीधर पाठक, लाला सीताराम, श्रद्धाराम फिल्लौरी, माधव प्रसाद मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि महान् साहित्यकारों को भुला दिया, वहाँ मैं यदि यह सोचूँ की हिंदीवाले मुझे सौ-पचास वर्ष भी याद रखेंगे तो मैं महामूर्खों की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता हूँ।
मैंने इन संस्मरणों को अपने उत्तराधिकारयों के लिए लिखा है। इसलिए इनकी केवल सौ प्रतियों छपाऊँगा। बीस-पचीस प्रतियाँ तो कुछ विशिष्ट मित्रों को दे दूँगा, शेष निजी पुस्तकालय में सुरक्षित रहेंगी उन्हें पढ़ने की लालसा केवल मेरे उत्तराधिकारियों को होगी। मेरे उत्तराधिकारी कौन हैं ? मेरे वंशज मेरे कानूनी उत्तराधिकारी मात्र हैं। वे मेरी भौतिक संपत्ति के (जो नगण्य है) उत्तराधिकारी हैं; किन्तु मेरे वास्तविक उत्तराधिकारी वे भावी युवक हैं जिनमें हिंदी-प्रेम ही नहीं, हिंदी का दर्द भी हो; वे नहीं जो मात्र साहित्य-रचना कर या संपादन या हिंदी अध्यापन कर अपना पेट पालते हों और इसी को हिन्दी-सेवा समझते हों। मेरे उत्तराधिकारी वे होंगे जो हिंदी के हितों, हिंदीभाषियों और हिंदी की सेवा करनेवालों के हितों के लिए निस्पृह भाव से कार्य करें और हिंदी-भक्त साहित्यकारों की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास करें और हिंदी के लिए त्याग और कठिन परीक्षा देने को तैयार हों और जो हिंदी के मान की प्राणपण से रक्षा करें तथा हिंदी का ‘अलमबरदार’ होना गौरव की बात समझें।
मुझमें जो भी हिंदी की निष्ठा है वह मैंने अपने पूज्य पिता जी, महामना मालवीयजी, पं. बालकृष्ण भट्ट और राजर्षि टंडन से पाई है। इस अर्थ में उनका ‘वारिस’ हूँ- चाहे कितना भी अयोग्य वारिश क्यों न होऊँ। किंतु मुझे उनके वारिस होने का गर्व है। मुझे जीवन की संध्या में इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी अल्पबुद्धि क्षीण सामर्थ्य और उपलब्ध अपर्याप्त साधनों का उनके दिखाए मार्ग पर हिंदी की सेवा में निस्पृह भाव से पूरा उपयोग करने का प्रयत्न किया*।
‘‘With a spoonful or bucketful of salt’
इसका कारण यह था कि मेरे पास इन प्रकरणों के लिए कोई प्रमाण न था। यदि मित्रवत पं. बलभद्र मिश्र ने उस प्रकरण के संबंध में लेख न लिखा होता जो उन्होंने लिखकर मुझे कहीं छापने के लिए दिया था (मैंने सेवा) में होने के कारण उसे उस समय छापना उचित नहीं समझा था) तथा 1976 में मित्रों द्वारा स्नेहवश प्रयाग में आयोजित सारस्वत समारोह के अवसर पर भाई सीताराम जाजू के हिन्दुस्तानी अकादमी के सचिव पं. उमाशंकर शुल्क को वह पत्र न भेजा होता जो मैंने अपने लेख में उद्धृत किया है (और जिसकी एक प्रतिलिपि हाथ से लिखकर मुझे भेजी), तो उसे मैं नहीं लिखता। मौखिक रूप से मैंने इनकी चर्चा (विशेषकर श्री जाजूवाले प्रसंग की) किसी से नहीं की किन्तु अब उन घटनाओं की सप्रमाण (विश्वासनीय व्यक्तियों की लिखित) साक्षी मिल जाने पर ही मैंने उन्हें लिपिबद्ध किया है। ऐसे अन्य प्रसंग भी हैं; किंतु मेरे पास उनके संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य नहीं हैं। यदि वे लोगों को कुछ मनोरंजन करें या कुछ प्रेरणा दें तो मेरे लिए पर्याप्त है।
हिन्दी की सेवा का अर्थ केवल साहित्य रचना नहीं है। मैंने अपने विचार से जिस काम को हिंदी के हित में समझा, वह किया।
साहित्य-रचना के क्षेत्र में मेरा काम उल्लेखनीय है या नहीं अथवा मेरा संपादन किसी काम का है या नहीं, इसकी चिंता मुझे नहीं। जिस हिंदी संसार ने श्रीधर पाठक, लाला सीताराम, श्रद्धाराम फिल्लौरी, माधव प्रसाद मिश्र, अंबिकादत्त व्यास आदि महान् साहित्यकारों को भुला दिया, वहाँ मैं यदि यह सोचूँ की हिंदीवाले मुझे सौ-पचास वर्ष भी याद रखेंगे तो मैं महामूर्खों की श्रेणी में आसानी से रखा जा सकता हूँ।
मैंने इन संस्मरणों को अपने उत्तराधिकारयों के लिए लिखा है। इसलिए इनकी केवल सौ प्रतियों छपाऊँगा। बीस-पचीस प्रतियाँ तो कुछ विशिष्ट मित्रों को दे दूँगा, शेष निजी पुस्तकालय में सुरक्षित रहेंगी उन्हें पढ़ने की लालसा केवल मेरे उत्तराधिकारियों को होगी। मेरे उत्तराधिकारी कौन हैं ? मेरे वंशज मेरे कानूनी उत्तराधिकारी मात्र हैं। वे मेरी भौतिक संपत्ति के (जो नगण्य है) उत्तराधिकारी हैं; किन्तु मेरे वास्तविक उत्तराधिकारी वे भावी युवक हैं जिनमें हिंदी-प्रेम ही नहीं, हिंदी का दर्द भी हो; वे नहीं जो मात्र साहित्य-रचना कर या संपादन या हिंदी अध्यापन कर अपना पेट पालते हों और इसी को हिन्दी-सेवा समझते हों। मेरे उत्तराधिकारी वे होंगे जो हिंदी के हितों, हिंदीभाषियों और हिंदी की सेवा करनेवालों के हितों के लिए निस्पृह भाव से कार्य करें और हिंदी-भक्त साहित्यकारों की स्मृति को जीवित रखने का प्रयास करें और हिंदी के लिए त्याग और कठिन परीक्षा देने को तैयार हों और जो हिंदी के मान की प्राणपण से रक्षा करें तथा हिंदी का ‘अलमबरदार’ होना गौरव की बात समझें।
मुझमें जो भी हिंदी की निष्ठा है वह मैंने अपने पूज्य पिता जी, महामना मालवीयजी, पं. बालकृष्ण भट्ट और राजर्षि टंडन से पाई है। इस अर्थ में उनका ‘वारिस’ हूँ- चाहे कितना भी अयोग्य वारिश क्यों न होऊँ। किंतु मुझे उनके वारिस होने का गर्व है। मुझे जीवन की संध्या में इस बात का संतोष है कि मैंने अपनी अल्पबुद्धि क्षीण सामर्थ्य और उपलब्ध अपर्याप्त साधनों का उनके दिखाए मार्ग पर हिंदी की सेवा में निस्पृह भाव से पूरा उपयोग करने का प्रयत्न किया*।
-श्रीनारायण चतुर्वेदी
* यह निवेदन पूज्य भैया ‘डिसमिसल और रेजिग्नेशन का
झगड़ा’ तथा
‘हिंदी को भारत की राजभाषा बनाने का उपक्रम’ लेखों की
भूमिका
के रूप में लिखा
था।
-संपादक
डिसमिसल और रेजिग्न्शन का झगड़ा
यह, संस्मरण लिखने के पहले मैं पाठकों को बता दूँ कि मेरे पूज्य पिताजी
सरकारी नौकरी में इलाहाबाद के सिविल सर्जन के कार्यालय में
हैडक्लर्क थे। कहावत है कि जब सियार की शामत आती है तब वह नगर की ओर भागता
है। इसी तरह जब किसी भले आदमी की शामत आती है तब वह साहित्य लिखने लगता
है। हमारे परिवार में लेखन की पुरानी परंपरा थी। एक पूर्वज आचार्य
गोविंददासजी ने ‘प्रपत्ति वैभव’ नाम की पुस्तक लिखी
थी। यह
विचित्र पुस्तक है। मूल व्रजभाषा में है और उसकी टीका संस्कृत में है।
उनके शिष्य मधुसूदनदासजी ने ‘रामाश्वमेध’ नामक
प्रसिद्ध ग्रंथ
लिखा है जिसके संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वह इतना
उत्कृष्ट है की तुलसीदासजी की रामायण का परिशिष्ट होने के योग्य है।
इसमें रामायण के बाद लवकुश की कथा है। एक दूसरे पूर्वज ने तुलसीदास की रामायण का संस्कृत में बड़ा उत्कृष्ट और सदभावनापूर्ण अनुवाद किया था।
मेरे चचेरे पितामाह सर रघुनाथदास चौबे केटी, सी.आई. ई. ने ‘भार्याहित नामक पुस्तक लिखी थी। एक चाचा ने डॉ. थीवो के ‘वेदांत दर्शन’ की बृहद् भूमिका (लगभग 250 पृष्ठ) का अनुवाद किया था। मेरे पितामाह और चाचा भी बड़े साहित्य-प्रेमी थे।
मेरे पिता जब तक प्रयाग नहीं गए तब तक उनके मस्तिष्क के साहित्यिक कीटाणु सुप्तावस्था में रहे। वहाँ पड़ोस मिला महामना मदनमोहन मालवीय और पं. बालकृष्ण भट्ट का और मित्रता हुई राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे लोगों से। अतएव साहित्यिक कीटाणु सक्रिय हो गए। उन्हें इतिहास में रुचि थी। पहले लार्ड क्लाइव की जीवनी लिखी, फिर वारेन हेस्टिंग्ज की। वे बड़े अध्ययनशील थे। बीसों अंग्रेजों की प्रामाणिक पुस्तकें जमा कीं और उनका अध्ययन किया। फिर वारेन हेस्टिंग्ज का एक बड़ा जीवनचरित्र लिख डाला और स्वयं प्रकाशित कर दिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने ‘ब्रूयात सत्यमप्रियम्’ का ध्यान नहीं रखा।
उस समय एक सरकारी रिपोर्टर हुआ करते थे जो प्रांत में प्रकाशित पुस्तकों की सूची बनाकर सरकारी गजट में छापते और जो रिपोर्ट करने योग्य पुस्तकें होतीं उन पर सरकार को रिपोर्ट भेजते। वे बड़े राजभक्त थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्ज के जीवनचरित्र के बीसों पृष्ठों को रेखांकित कर सरकार को भेजा और लिखा कि वह अंग्रेज विरोधी पुस्तक है। उस पर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के सिविल सर्जन कर्नल मेकलारेन को लिखा कि यदि आपका हैडक्लर्क इस पुस्तक का लेखक होना स्वीकार कर ले तो उसे सेवा से तत्काल डिसमिस कर दीजिए।
कर्नल मेकलारेन पिताजी को बहुत मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। यह पत्र सवेरे की डाक से उसके घर पहुँचा। जब पिताजी दस बजे कार्यालय पहुँचे तो कर्नल साहब ने उनसे कहा कि काम समाप्त होने पर घर जाने से पहले मुझसे मिल लेना। अतएव संध्या को पाँच बजे जब कार्यालय में ताला लगा दिया तो वे उनके पास गए। उन्होंने उनसे सामने की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और बोले, ‘‘क्या आपने ‘वारेन हेस्टिंग्ज का जीवनचरित्र’ नामक कोई पुस्तक लिखी है ?’’
पिताजी के ‘हाँ’ कहने पर उन्होंने बिना कुछ कहे श्री होज का पत्र उनके सामने रख दिया। जब उन्होंने पत्र पढ़ लिया तो वे बोले, ‘‘मुझे बड़ा दुःख है।
किंतु ये गवर्नमेंट के आदेश हैं और इनका पालन न करना मेरी शक्ति से बाहर है।’’ पिताजी ने कहा यह तो भाग्य की बात है। किसी का दोष नहीं,’’ और कार्यालय की तालियाँ देकर अपनी साइकिल लेकर घर चले आए। घर पर उन्होंने किसी से यह बात नहीं कही, केवल कार्यालय जाना बन्द कर दिया।
दूसरे दिन कर्नल साहब ने चपरासी भेजकर मिलने के लिए उन्हें बुलाया और कहा कि सरकारी नौकरी दिलाना तो मेरी सामर्थ्य से परे है, किंतु यहाँ बी. एन. डब्ल्यू. रेलवे की लाइन बनारस से आ रही है और उसका पुल दारागंज में बन भी गया है। यह एक अंग्रेज कंपनी की रेल है। मैं उसके अनेक उच्च अधिकारियों को जानता हूँ और उनसे कहकर आपको उस रेल कंपनी में कोई नौकरी दिला सकता हूँ।
किंतु पिता ने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा।
कर्नल साहब ने कहा, ‘‘अभी आप इस आकस्मिक दुर्घटना से उद्धिग्न और विचलित हैं। कोई जल्दी नहीं है। आप खूब सोच लें। जब आप निश्चय कर लें तब बताएँ। मैं आपको वहाँ कोई अच्छी नौकरी दिला दूँगा।’’
पिताजी उनकी सहानुभूति और कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देकर लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने गंगाजी के किनारे एक कुटिया (झोपड़ी) बनवाकर गायत्री मंत्र का सवा लक्ष का अनुष्ठान आरंभ कर दिया जो प्रायः बीस दिन चला। उसके बाद हवन आदि हुआ। नौकरी की बात दिमाग से एकदम निकल गई। वे आजीवन साहित्य सेवा में (चार आना पृष्ठ पर) पुस्तकें लिखकर हम सबका पालन-पोषण करते रहे। उपर्युक्त घटना का यहाँ उल्लेख इसलिए आवश्यक है ताकि पाठकों को मेरे संस्कार और पृष्ठभूमि का परिचय मिल जाए, यद्यपि इसका उस घटना से कोई संबंध नहीं है, जिसे मैं लिखने जा रहा हूँ।
सन् 1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित हुई। 1934 से मैं फैजाबाद का डिवीजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था। जब पुरानी सरकार ने लखनऊ में एक बृहद् प्रांतीय प्रदर्शनी आयोजित की तब मुझे स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करके उसके एजूकेशन कोर्ट का प्रभारी अधिकारी बनाया गया। वह कोर्ट इतना महत्त्वपूर्ण और दर्शनीय समझा गया कि जब तत्कालीन गवर्नर सर हेरी हेग प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए तो चार कोर्ट उन्हें दिखाए गए उनमें एक एजूकेशन कोर्ट भी था।
उसकी सफलता से मेरी भी कुछ ख्याति हो गई। इसलिए जब नई कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देवजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई तब मैं और डॉ. इवादुर्रहमान खाँ उसके सचिव नियुक्त किये गए। इस समिति के एक सदस्य डॉ. जाकिर हुसैन भी थे, जो गांधीजी की बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ माने जाते थे। कमेटी का काम पूरा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस सरकार ने कई जनोपयोगी योजनाएँ आरंभ कीं। उनमें मेरी दृष्टि से दो विशेष उल्लेखनीय थीं- एक तो ग्राम्य विकास (रूरल डेवलपमेंट) और दूसरी शिक्षा प्रसार।
पहली योजना का उद्देश्य गाँवों का संपूर्ण और बहुमुखी विकास था, तथा दूसरी का प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, नवसाक्षरों और गाँवों के शिक्षित लोगों के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय खोलना और उन्हें चलाना था।
पहले मैं इस योजना को तैयार करने के लिए सचिवालय में स्पेशल डयूटी पर रखा गया और फिर जब सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया तब एक नया विभाग-शिक्षा प्रसार विभाग-बनाकर मुझे शिक्षा प्रसार अधिकारी के नाम से उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले मेरा कार्यालय लखनऊ में सचिवालय में था। फिर वह इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
यद्यपि मैं अपने विभाग का काम करने के लिए स्वतंत्र था, फिर भी स्थायी डिविजनल इंस्पेक्टर होने के कारण औपचारिक रूप से शिक्षा निदेशक के अधीन था। मैंने 1,200 पुस्तकालय 3,600 वाचनालय खोले तथा प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए कई रात्रि पाठशालाएँ खोलीं। इनमें सामान्यतः हिंदी की आरंभिक शिक्षा दी जाती थी। वाचनालय में दो साप्ताहिक पत्रिकाएँ दी जाती थीं। पाठकों की सुविधा, सहायता तथा वाचनालयों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें एक अच्छा हिंदीकोश, वर्ष पंचांग (जिससे गाँव के लोंगों को पर्व और तिथियाँ मालूम हो सकें) तथा उस जिले में चलनेवाली रेल की समय सारिणी (जो उन दिनों टाइम टेबल ऑफिस, बनारस से हिंदी में छपती थी) दी गई। इसके अतिरिक्त दो समाचार-प्रधान साप्ताहिक भी देने का प्रबंध था। पुस्तकालय में रामायण आदि ग्रंथों के साथ–साथ मनोरंजक और उपयोगी पुस्तकों की भी अच्छी व्यवस्था थी। रात्रि पाठशालाओं में स्थानीय अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए भत्ता दिया जाता था तथा आवश्यक प्रौढ़ोपयोगी पुस्तकें, चार्ट, बिछौने तथा लालटेनें भी दी जाती थीं। 90 प्रतिशत रात्रि पाठशालाओं में हिंदी पढा़ई जाती थी। कहीं-कहीं, जहाँ माँग हुई, उर्दू पढ़ाने का भी प्रबंध था।
यह कार्य सुचारू रूप से चल निकला। उसके प्रचार के लिए समय-समय पर आकर्षक पोस्टर तथा टिकट आदि निकाले जाने लगे। किंतु 1939 में द्विताय विश्वयुद्ध के छिड़ने पर राजनैतिक कारणों से कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैलट साहब थे। राज्य गवर्नर शासन हो गया। उन्होंने भी श्री पन्नावलाल आई. सी. एस. और श्री शेरिफ आई. सी. एस. को अपना सलाहकार बनाया। शिक्षा विभाग के प्रशासन का भार श्री शेरिफ को सौंपा गया।
श्री शेरिफ मेरे विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हो गए। किंतु मैं उनसे मिलने नहीं गया। मैं कभी बिना बुलाए अफसरों से मिलने नहीं जाता था। अफसरों से शायद अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नए उच्च अधिकारियों पर Call करेंगे।
प्रशासनिक दृष्टि से यह ठीक भी है। इससे एक दूसरे को जान जाते हैं। किंतु मैं स्वभाव से कुछ आलसी हूँ और ‘सलाम’ करने जाना (जिसे अधिनस्थ अधिकारी Call करना कहते हैं) मुझे पसंद नहीं। मैंने कहावत सुनी थी हाथी के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी से दूर रहे। मैंने इसको सुधाकर बदल दिया ‘अफसर के अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों से दूर रहे’ मैं आज अनुभव करता हूँ कि मेरा विचार गलत था। कुछ अधिकारी मुझे ‘मगरूर’ समझने लगे। कुछ मुझे डरपोक समझने लगे। मेरी आदत से मुझे अनेक बार तरह-तरह की हानियाँ भी उठानी पड़ीं। मैं दूसरों को अपना अनुकरण करने की सलाह न दूँगा। जो भी हो मेरे विभाग का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था। किंतु 1940 के उत्तरार्द्ध में अनभ्र आकाश से वज्रपात होने की तरह मुझे लखनऊ से सरकार का एक आदेश मिला। वह आदेश यह था कि रात्रि पाठशालाओं में जो हिंदी आरंभिक शिक्षा दी जाती है, उसे सरकार ने रोमन अक्षरों से देने के निर्णय किया है। मैं इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध आरंभ कर दूँ।
इस आदेश को पढ़कर मैं विचलित हो गया। युद्ध का समय, हैलट साहब की सरकार, सरकार का आदेश और मैं शिक्षा विभाग के एक छोटे अंश का सामान्य अधिकारी ! दूसरी ओर महामना, राजर्षि और पूज्य पिताजी से प्राप्त भाषा और लिपि संबंधी गहरे संस्कार ! विडंबना य़ह कि अशिव कार्य को करने-देवनागरी के बजाय रोमन लिपि का अप्रिय और भाषा-विरोधी काम करने का भार इतने बड़े शिक्षा विभाग में मुझे दिया गया। उसे करने का मतलब था सारे जीवन की मातृभाषा संबंधी सभी मान्यताओं को नकारना। मैं किंकर्तव्यविमूढ हो गया। कई दिन चिंता के मारे नींद नहीं आई।
अंत में मैंने शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें इस परिवर्तन में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों का वर्णन था। रोमन में हिंदी की आरंभिक पुस्तकें नहीं थीं। उनको तैयार करना और छपाना कठिन और समय-साध्य कार्य था। नवसाक्षरों को यदि पढ़ने के लिए प्रचुर साहित्य नहीं दिया जाए तो वे फिर निरक्षर हो जाएँगे। रोमन में वैसा साहित्य नहीं था। उसे प्रचुर मात्रा में तैयार करना और भी कठिन था।
नवसाक्षर देवनागरी न जानने के कारण हिंदी में छपे अपार साहित्य को पढ़ न सकेंगे और रामायण आदि न पढ़ सकने के कारण उनके साक्षर होने का एक बड़ा ‘मोटिव’ पूरा न होगा। रात्रि पाठशालाओं में पढ़ने आना उनकी इच्छा पर था। रोमन लिपि में हिंदी पढ़ने वे या तो आएँगे ही नहीं और यदि आए भी तो एक-दो की संख्या में। सबसे बड़ी कठिनाई थी इन सैकड़ों रात्रि पाठशालाओं में या तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक या गाँव के मिडिल पास व्यक्ति नाम मात्र का भत्ता लेकर पढ़ते थे। गाँवों में और इन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों में रोमन लिपि जाननेवाले की अव्यावहारिकता का वर्णन कर उसे असाध्य बताने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पत्र में केवल प्रशासनिक कठिनाइयाँ ही लिखी थीं। सिद्धांत की कोई बात न लिखी थी। किंतु सरकार पर इस पत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। केवल यह उत्तर आया कि सरकार इन सब बातों को समझती है। धीरे-धीरे सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। अतः आदेशों का तुरंत पालन करूँ।
मैंने इस पर एक दूसरा पत्र लिखा। इसमें मैंने कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन करके यह बतलाया कि इस योजना से जनता में बड़ा असंतोष होगा और आंदोलनकारी इसका लाभ उठाकर एक नया आंदोलन आरंभ कर देंगे, जो सरकार के लिए सिरदर्द हो जाएगा। इस बार मैंने यह पत्र तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री पॉवल प्राइस को दिखाकर उनके माध्यम से भिजवाया; क्योंकि मैं तो वास्तव में शिक्षा निदेशक के अधीन था और वे सारे शिक्षा विभाग के लिए उत्तरदायी थे। सौभाग्य से वे मुझसे सहमत थे और उन्होंने अपनी आख्या के साथ उसे सरकार को भेज दिया। उन्होंने जो लिखा उसका सारांश यह था कि लिपि परिवर्तन का प्रस्ताव कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसे अब लागू करना संभव नहीं। यदि वह कुछ दशक पूर्व आरंभ किया जाता तो उसकी सफलता की संभावना थी।
इस पत्र का कोई उत्तर नहीं, किंतु मुझे आदेश हुआ कि मैं लखनऊ जाकर गवर्नर के शिक्षा सलाहकार श्री शेरिफ से मिलूँ। अतएव मैं धुकधुकाते हृदय से लखनऊ गया। मैं उस समय सरकार की शक्ति और दृढ़ता को जानता था तथा अपने विचार की गहराई को भी। मैं स्पष्टवादिता के लिए बदनाम रही हूँ। वैसे तो मैं अपने ऊपर संयम रखता हूँ, किंतु अब उत्तेजित होता हूँ तो फिर दूसरे व्यक्ति के पद और अपने पद को भूलकर जो मन में आता है, वह बक जाता हूँ।
इसमें रामायण के बाद लवकुश की कथा है। एक दूसरे पूर्वज ने तुलसीदास की रामायण का संस्कृत में बड़ा उत्कृष्ट और सदभावनापूर्ण अनुवाद किया था।
मेरे चचेरे पितामाह सर रघुनाथदास चौबे केटी, सी.आई. ई. ने ‘भार्याहित नामक पुस्तक लिखी थी। एक चाचा ने डॉ. थीवो के ‘वेदांत दर्शन’ की बृहद् भूमिका (लगभग 250 पृष्ठ) का अनुवाद किया था। मेरे पितामाह और चाचा भी बड़े साहित्य-प्रेमी थे।
मेरे पिता जब तक प्रयाग नहीं गए तब तक उनके मस्तिष्क के साहित्यिक कीटाणु सुप्तावस्था में रहे। वहाँ पड़ोस मिला महामना मदनमोहन मालवीय और पं. बालकृष्ण भट्ट का और मित्रता हुई राजर्षि पुरुषोत्तमदास टंडन जैसे लोगों से। अतएव साहित्यिक कीटाणु सक्रिय हो गए। उन्हें इतिहास में रुचि थी। पहले लार्ड क्लाइव की जीवनी लिखी, फिर वारेन हेस्टिंग्ज की। वे बड़े अध्ययनशील थे। बीसों अंग्रेजों की प्रामाणिक पुस्तकें जमा कीं और उनका अध्ययन किया। फिर वारेन हेस्टिंग्ज का एक बड़ा जीवनचरित्र लिख डाला और स्वयं प्रकाशित कर दिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए भी उन्होंने ‘ब्रूयात सत्यमप्रियम्’ का ध्यान नहीं रखा।
उस समय एक सरकारी रिपोर्टर हुआ करते थे जो प्रांत में प्रकाशित पुस्तकों की सूची बनाकर सरकारी गजट में छापते और जो रिपोर्ट करने योग्य पुस्तकें होतीं उन पर सरकार को रिपोर्ट भेजते। वे बड़े राजभक्त थे। उन्होंने वारेन हेस्टिंग्ज के जीवनचरित्र के बीसों पृष्ठों को रेखांकित कर सरकार को भेजा और लिखा कि वह अंग्रेज विरोधी पुस्तक है। उस पर तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी ने इलाहाबाद के सिविल सर्जन कर्नल मेकलारेन को लिखा कि यदि आपका हैडक्लर्क इस पुस्तक का लेखक होना स्वीकार कर ले तो उसे सेवा से तत्काल डिसमिस कर दीजिए।
कर्नल मेकलारेन पिताजी को बहुत मानते थे और उनका बड़ा आदर करते थे। यह पत्र सवेरे की डाक से उसके घर पहुँचा। जब पिताजी दस बजे कार्यालय पहुँचे तो कर्नल साहब ने उनसे कहा कि काम समाप्त होने पर घर जाने से पहले मुझसे मिल लेना। अतएव संध्या को पाँच बजे जब कार्यालय में ताला लगा दिया तो वे उनके पास गए। उन्होंने उनसे सामने की कुर्सी पर बैठने के लिए कहा और बोले, ‘‘क्या आपने ‘वारेन हेस्टिंग्ज का जीवनचरित्र’ नामक कोई पुस्तक लिखी है ?’’
पिताजी के ‘हाँ’ कहने पर उन्होंने बिना कुछ कहे श्री होज का पत्र उनके सामने रख दिया। जब उन्होंने पत्र पढ़ लिया तो वे बोले, ‘‘मुझे बड़ा दुःख है।
किंतु ये गवर्नमेंट के आदेश हैं और इनका पालन न करना मेरी शक्ति से बाहर है।’’ पिताजी ने कहा यह तो भाग्य की बात है। किसी का दोष नहीं,’’ और कार्यालय की तालियाँ देकर अपनी साइकिल लेकर घर चले आए। घर पर उन्होंने किसी से यह बात नहीं कही, केवल कार्यालय जाना बन्द कर दिया।
दूसरे दिन कर्नल साहब ने चपरासी भेजकर मिलने के लिए उन्हें बुलाया और कहा कि सरकारी नौकरी दिलाना तो मेरी सामर्थ्य से परे है, किंतु यहाँ बी. एन. डब्ल्यू. रेलवे की लाइन बनारस से आ रही है और उसका पुल दारागंज में बन भी गया है। यह एक अंग्रेज कंपनी की रेल है। मैं उसके अनेक उच्च अधिकारियों को जानता हूँ और उनसे कहकर आपको उस रेल कंपनी में कोई नौकरी दिला सकता हूँ।
किंतु पिता ने कहा कि अब मैं नौकरी नहीं करूँगा।
कर्नल साहब ने कहा, ‘‘अभी आप इस आकस्मिक दुर्घटना से उद्धिग्न और विचलित हैं। कोई जल्दी नहीं है। आप खूब सोच लें। जब आप निश्चय कर लें तब बताएँ। मैं आपको वहाँ कोई अच्छी नौकरी दिला दूँगा।’’
पिताजी उनकी सहानुभूति और कृपा के लिए उन्हें धन्यवाद देकर लौट आए। दूसरे दिन उन्होंने गंगाजी के किनारे एक कुटिया (झोपड़ी) बनवाकर गायत्री मंत्र का सवा लक्ष का अनुष्ठान आरंभ कर दिया जो प्रायः बीस दिन चला। उसके बाद हवन आदि हुआ। नौकरी की बात दिमाग से एकदम निकल गई। वे आजीवन साहित्य सेवा में (चार आना पृष्ठ पर) पुस्तकें लिखकर हम सबका पालन-पोषण करते रहे। उपर्युक्त घटना का यहाँ उल्लेख इसलिए आवश्यक है ताकि पाठकों को मेरे संस्कार और पृष्ठभूमि का परिचय मिल जाए, यद्यपि इसका उस घटना से कोई संबंध नहीं है, जिसे मैं लिखने जा रहा हूँ।
सन् 1937 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार स्थापित हुई। 1934 से मैं फैजाबाद का डिवीजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स था। जब पुरानी सरकार ने लखनऊ में एक बृहद् प्रांतीय प्रदर्शनी आयोजित की तब मुझे स्पेशल ऑफिसर नियुक्त करके उसके एजूकेशन कोर्ट का प्रभारी अधिकारी बनाया गया। वह कोर्ट इतना महत्त्वपूर्ण और दर्शनीय समझा गया कि जब तत्कालीन गवर्नर सर हेरी हेग प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए तो चार कोर्ट उन्हें दिखाए गए उनमें एक एजूकेशन कोर्ट भी था।
उसकी सफलता से मेरी भी कुछ ख्याति हो गई। इसलिए जब नई कांग्रेस सरकार ने शिक्षा के सुधार के लिए आचार्य नरेंद्र देवजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई तब मैं और डॉ. इवादुर्रहमान खाँ उसके सचिव नियुक्त किये गए। इस समिति के एक सदस्य डॉ. जाकिर हुसैन भी थे, जो गांधीजी की बेसिक शिक्षा के विशेषज्ञ माने जाते थे। कमेटी का काम पूरा भी नहीं हुआ था कि कांग्रेस सरकार ने कई जनोपयोगी योजनाएँ आरंभ कीं। उनमें मेरी दृष्टि से दो विशेष उल्लेखनीय थीं- एक तो ग्राम्य विकास (रूरल डेवलपमेंट) और दूसरी शिक्षा प्रसार।
पहली योजना का उद्देश्य गाँवों का संपूर्ण और बहुमुखी विकास था, तथा दूसरी का प्रौढ़ों को साक्षर बनाना, नवसाक्षरों और गाँवों के शिक्षित लोगों के लिए पुस्तकालय तथा वाचनालय खोलना और उन्हें चलाना था।
पहले मैं इस योजना को तैयार करने के लिए सचिवालय में स्पेशल डयूटी पर रखा गया और फिर जब सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया तब एक नया विभाग-शिक्षा प्रसार विभाग-बनाकर मुझे शिक्षा प्रसार अधिकारी के नाम से उसका अध्यक्ष बनाया गया। पहले मेरा कार्यालय लखनऊ में सचिवालय में था। फिर वह इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया।
यद्यपि मैं अपने विभाग का काम करने के लिए स्वतंत्र था, फिर भी स्थायी डिविजनल इंस्पेक्टर होने के कारण औपचारिक रूप से शिक्षा निदेशक के अधीन था। मैंने 1,200 पुस्तकालय 3,600 वाचनालय खोले तथा प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए कई रात्रि पाठशालाएँ खोलीं। इनमें सामान्यतः हिंदी की आरंभिक शिक्षा दी जाती थी। वाचनालय में दो साप्ताहिक पत्रिकाएँ दी जाती थीं। पाठकों की सुविधा, सहायता तथा वाचनालयों को अधिक उपयोगी बनाने के लिए उनमें एक अच्छा हिंदीकोश, वर्ष पंचांग (जिससे गाँव के लोंगों को पर्व और तिथियाँ मालूम हो सकें) तथा उस जिले में चलनेवाली रेल की समय सारिणी (जो उन दिनों टाइम टेबल ऑफिस, बनारस से हिंदी में छपती थी) दी गई। इसके अतिरिक्त दो समाचार-प्रधान साप्ताहिक भी देने का प्रबंध था। पुस्तकालय में रामायण आदि ग्रंथों के साथ–साथ मनोरंजक और उपयोगी पुस्तकों की भी अच्छी व्यवस्था थी। रात्रि पाठशालाओं में स्थानीय अध्यापकों को प्रौढ़ शिक्षा देने के लिए भत्ता दिया जाता था तथा आवश्यक प्रौढ़ोपयोगी पुस्तकें, चार्ट, बिछौने तथा लालटेनें भी दी जाती थीं। 90 प्रतिशत रात्रि पाठशालाओं में हिंदी पढा़ई जाती थी। कहीं-कहीं, जहाँ माँग हुई, उर्दू पढ़ाने का भी प्रबंध था।
यह कार्य सुचारू रूप से चल निकला। उसके प्रचार के लिए समय-समय पर आकर्षक पोस्टर तथा टिकट आदि निकाले जाने लगे। किंतु 1939 में द्विताय विश्वयुद्ध के छिड़ने पर राजनैतिक कारणों से कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दे दिया। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैलट साहब थे। राज्य गवर्नर शासन हो गया। उन्होंने भी श्री पन्नावलाल आई. सी. एस. और श्री शेरिफ आई. सी. एस. को अपना सलाहकार बनाया। शिक्षा विभाग के प्रशासन का भार श्री शेरिफ को सौंपा गया।
श्री शेरिफ मेरे विभाग के सबसे बड़े अधिकारी हो गए। किंतु मैं उनसे मिलने नहीं गया। मैं कभी बिना बुलाए अफसरों से मिलने नहीं जाता था। अफसरों से शायद अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नए उच्च अधिकारियों पर Call करेंगे।
प्रशासनिक दृष्टि से यह ठीक भी है। इससे एक दूसरे को जान जाते हैं। किंतु मैं स्वभाव से कुछ आलसी हूँ और ‘सलाम’ करने जाना (जिसे अधिनस्थ अधिकारी Call करना कहते हैं) मुझे पसंद नहीं। मैंने कहावत सुनी थी हाथी के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी से दूर रहे। मैंने इसको सुधाकर बदल दिया ‘अफसर के अगाड़ी और पिछाड़ी दोनों से दूर रहे’ मैं आज अनुभव करता हूँ कि मेरा विचार गलत था। कुछ अधिकारी मुझे ‘मगरूर’ समझने लगे। कुछ मुझे डरपोक समझने लगे। मेरी आदत से मुझे अनेक बार तरह-तरह की हानियाँ भी उठानी पड़ीं। मैं दूसरों को अपना अनुकरण करने की सलाह न दूँगा। जो भी हो मेरे विभाग का कार्य सुचारु रूप से चल रहा था। किंतु 1940 के उत्तरार्द्ध में अनभ्र आकाश से वज्रपात होने की तरह मुझे लखनऊ से सरकार का एक आदेश मिला। वह आदेश यह था कि रात्रि पाठशालाओं में जो हिंदी आरंभिक शिक्षा दी जाती है, उसे सरकार ने रोमन अक्षरों से देने के निर्णय किया है। मैं इसे क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक प्रबंध आरंभ कर दूँ।
इस आदेश को पढ़कर मैं विचलित हो गया। युद्ध का समय, हैलट साहब की सरकार, सरकार का आदेश और मैं शिक्षा विभाग के एक छोटे अंश का सामान्य अधिकारी ! दूसरी ओर महामना, राजर्षि और पूज्य पिताजी से प्राप्त भाषा और लिपि संबंधी गहरे संस्कार ! विडंबना य़ह कि अशिव कार्य को करने-देवनागरी के बजाय रोमन लिपि का अप्रिय और भाषा-विरोधी काम करने का भार इतने बड़े शिक्षा विभाग में मुझे दिया गया। उसे करने का मतलब था सारे जीवन की मातृभाषा संबंधी सभी मान्यताओं को नकारना। मैं किंकर्तव्यविमूढ हो गया। कई दिन चिंता के मारे नींद नहीं आई।
अंत में मैंने शिक्षा सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें इस परिवर्तन में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों का वर्णन था। रोमन में हिंदी की आरंभिक पुस्तकें नहीं थीं। उनको तैयार करना और छपाना कठिन और समय-साध्य कार्य था। नवसाक्षरों को यदि पढ़ने के लिए प्रचुर साहित्य नहीं दिया जाए तो वे फिर निरक्षर हो जाएँगे। रोमन में वैसा साहित्य नहीं था। उसे प्रचुर मात्रा में तैयार करना और भी कठिन था।
नवसाक्षर देवनागरी न जानने के कारण हिंदी में छपे अपार साहित्य को पढ़ न सकेंगे और रामायण आदि न पढ़ सकने के कारण उनके साक्षर होने का एक बड़ा ‘मोटिव’ पूरा न होगा। रात्रि पाठशालाओं में पढ़ने आना उनकी इच्छा पर था। रोमन लिपि में हिंदी पढ़ने वे या तो आएँगे ही नहीं और यदि आए भी तो एक-दो की संख्या में। सबसे बड़ी कठिनाई थी इन सैकड़ों रात्रि पाठशालाओं में या तो प्राइमरी स्कूल के अध्यापक या गाँव के मिडिल पास व्यक्ति नाम मात्र का भत्ता लेकर पढ़ते थे। गाँवों में और इन प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों में रोमन लिपि जाननेवाले की अव्यावहारिकता का वर्णन कर उसे असाध्य बताने का प्रयत्न किया। मैंने अपने पत्र में केवल प्रशासनिक कठिनाइयाँ ही लिखी थीं। सिद्धांत की कोई बात न लिखी थी। किंतु सरकार पर इस पत्र का कोई प्रभाव न पड़ा। केवल यह उत्तर आया कि सरकार इन सब बातों को समझती है। धीरे-धीरे सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएँगी। अतः आदेशों का तुरंत पालन करूँ।
मैंने इस पर एक दूसरा पत्र लिखा। इसमें मैंने कठिनाइयों का संक्षिप्त वर्णन करके यह बतलाया कि इस योजना से जनता में बड़ा असंतोष होगा और आंदोलनकारी इसका लाभ उठाकर एक नया आंदोलन आरंभ कर देंगे, जो सरकार के लिए सिरदर्द हो जाएगा। इस बार मैंने यह पत्र तत्कालीन शिक्षा निदेशक श्री पॉवल प्राइस को दिखाकर उनके माध्यम से भिजवाया; क्योंकि मैं तो वास्तव में शिक्षा निदेशक के अधीन था और वे सारे शिक्षा विभाग के लिए उत्तरदायी थे। सौभाग्य से वे मुझसे सहमत थे और उन्होंने अपनी आख्या के साथ उसे सरकार को भेज दिया। उन्होंने जो लिखा उसका सारांश यह था कि लिपि परिवर्तन का प्रस्ताव कितना ही अच्छा क्यों न हो, उसे अब लागू करना संभव नहीं। यदि वह कुछ दशक पूर्व आरंभ किया जाता तो उसकी सफलता की संभावना थी।
इस पत्र का कोई उत्तर नहीं, किंतु मुझे आदेश हुआ कि मैं लखनऊ जाकर गवर्नर के शिक्षा सलाहकार श्री शेरिफ से मिलूँ। अतएव मैं धुकधुकाते हृदय से लखनऊ गया। मैं उस समय सरकार की शक्ति और दृढ़ता को जानता था तथा अपने विचार की गहराई को भी। मैं स्पष्टवादिता के लिए बदनाम रही हूँ। वैसे तो मैं अपने ऊपर संयम रखता हूँ, किंतु अब उत्तेजित होता हूँ तो फिर दूसरे व्यक्ति के पद और अपने पद को भूलकर जो मन में आता है, वह बक जाता हूँ।
|
|||||
अन्य पुस्तकें
लोगों की राय
No reviews for this book


 i
i